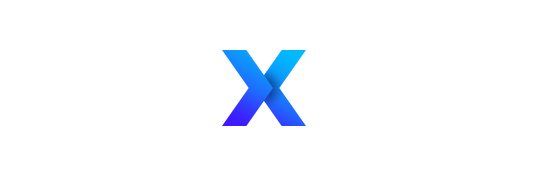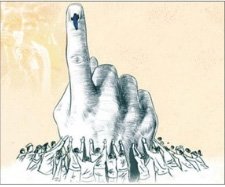चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होते हैं, लेकिन अपने देश में मतदान का प्रतिशत प्राय: कम रहता है। देश के पहले लोकसभा चुनाव में 1951-52 में मतदान का प्रतिशत 45 ही था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह 67 प्रतिशत हो गया। बेशक प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसे उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मतदान जनतंत्र का विशिष्ट अधिकार है, लेकिन यह एक पवित्र कर्तव्य भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी मतदान के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमें संकल्प लेना चाहिए कि मतदाता पीछे न रह जाएं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का प्रतिशत 67.40 था। मतदान के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मूलभूत प्रश्न है कि मतदान का प्रतिशत अभी भी उत्साहवर्द्धक स्थिति में क्यों नहीं है? क्या विभिन्न दलों के घोषणा पत्र व जनहितकारी आश्वासन मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते? अब मतदान के लिए तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पोलिंग बूथ भी घर से बहुत दूरी पर नहीं होते। राजनीतिक दलों के आश्वासन और किये गये काम विभिन्न संचार माध्यमों में सहज-शुलभ हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता।
चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होते हैं, लेकिन अपने देश में मतदान का प्रतिशत प्राय: कम रहता है। देश के पहले लोकसभा चुनाव में 1951-52 में मतदान का प्रतिशत 45 ही था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह 67 प्रतिशत हो गया। बेशक प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसे उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मतदान जनतंत्र का विशिष्ट अधिकार है, लेकिन यह एक पवित्र कर्तव्य भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी मतदान के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमें संकल्प लेना चाहिए कि मतदाता पीछे न रह जाएं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का प्रतिशत 67.40 था। मतदान के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मूलभूत प्रश्न है कि मतदान का प्रतिशत अभी भी उत्साहवर्द्धक स्थिति में क्यों नहीं है? क्या विभिन्न दलों के घोषणा पत्र व जनहितकारी आश्वासन मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते? अब मतदान के लिए तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पोलिंग बूथ भी घर से बहुत दूरी पर नहीं होते। राजनीतिक दलों के आश्वासन और किये गये काम विभिन्न संचार माध्यमों में सहज-शुलभ हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता।
चुनाव के दौरान सभी दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। सत्ता में आने पर तमाम योजनाओं के पूरा करने के आश्वासन देते हैं। मतदाताओं के सामने विकल्प की कमी नहीं है। दलों का चरित्र भी मजेदार है। अनेक दल विकास के वायदे करते हैं। विकास के इन वायदों पर मतदाता विश्वास नहीं करते। चुनाव में मुफ्त सामग्री देने जैसे वायदे भी होते हैं। चुनाव में मुफ्त वस्तु वितरण के वायदे का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ एक दल विचारधारा के आधार पर भी अपने चुनाव अभियान चलाते हैं, लेकिन मतदाताओं के बीच विचार का प्रभाव प्राय: नहीं दिखाई पड़ता है। जाति मजहब के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जाति और मजहब का उन्माद बढ़ाते हैं। सुधी मतदाता इससे आहत होते हैं और मतदान के प्रति उदासीन हो जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। प्रचार में बेमतलब के सवाल मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते।
चुनाव में मूलभूत प्रश्नों पर बहस करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। बेरोजगारी, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था, बिजली, पानी और सड़क जैसे मूलभूत प्रश्नों पर चुनाव में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चर्चा का अभाव है। विकास की आधारभूत संरचना भी चुनाव में बहस का मुद्दा नहीं है। जाति मजहब के आधार पर जारी चुनाव अभियान समाज का वातावरण बिगाड़ते हैं। ऐसे अभियान समाज की आधारभूत एकता पर भी चोट करते हैं। मूलभूत प्रश्न है कि हम वोट क्यों दें? क्या जाति की लामबंदी के लिए वोट दें? क्या राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों की उपेक्षा के बावजूद किसी दल को जाति मजहब के कारण वोट देना ठीक है? भारत के संविधान निर्माताओं ने लम्बी बहस के बाद संसदीय जनतंत्र अपनाया है। यहां प्रत्येक वयस्क को मताधिकार है। निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक चुनाव में अपील भी की जाती है, लेकिन मतदाता ऐसी अपीलों से प्रेरित नहीं होते।
मतदान के गर्भ से ही सरकार का जन्म होता है और विपक्ष का भी। मतदाता ही किसी दल को बहुमत और किसी दूसरे दल या समूह को अल्पमत देते हैं। बहुमत दल को शासन का अधिकार भी मतदाता ही देते हैं और विपक्ष को सरकारी काम की आलोचना का काम भी मतदाता ही सौंपते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि मतदाता भारी संख्या में मतदान करें। भारी संख्या से स्पष्ट जनादेश प्राप्त होता है। कम मतदान का अर्थ बड़ा सीधा और सरल है कि दलतंत्र के वायदे मतदाता को भारी मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते। राजनीति के प्रति आमजनों की घटती निष्ठा और बढ़ती उपेक्षा कम मतदान का कारण है।
लोकतंत्र भारत के लोगों की जीवनशैली है। यहां वैदिककाल से लेकर अब तक लोकतंत्र के प्रति गहरी निष्ठा है। संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से भिन्न है। इसकी उद्देशिका बार-बार पठनीय है। उद्देशिका के अनुसार संविधान की सर्वोपरिता का मुख्य श्रोत ‘हम भारत के लोग’ हैं। उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय समता व बंधुता के राष्ट्रीय स्वप्न हैं। चुनाव अभियान में संविधान की भावना के अनुसार बहस होनी चाहिए। इसी तरह संविधान में नीति-निर्देशक तत्व हैं और मूल कत्र्तव्य भी हैं। चुनाव अभियान में नीति-निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन पर बहस होनी चाहिए और मूल कर्तव्यों के पालन पर भी। लेकिन चुनाव अभियान में ऐसे उदत आदर्श नहीं दिखाई पड़ते। दलतंत्र को भारत की समृद्धि के लिए चुनावी बहस करनी चाहिए।
चुनाव भारतीय लोकतंत्र का असाधारण उत्सव है। भारी मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी दल अपनी विचार धारा के अनुसार चुनाव में हिस्सा लेतें हैं। सत्ता की दावेदारी भी करते हैं । चुनाव जनतंत्र के विचार व्यवहार व नीति कार्यक्रम की परीक्षा का अवसर होते हैं। चुनाव में सभी दलों को अपनी विचार धारा के प्रचार का अवसर मिलता है। भारत के कुछ दल जाति, गोत्र, वंश के आधार पर अभियान चलाते हैं। कुछ दलों के संस्थापक प्राय: आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों के न रहने के बाद उनके पुत्र या पुत्रियाँ पार्टी प्रापर्टी के मालिक हो जाते हैं। इससे लोकतंत्र की क्षति होती है। अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जिन दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ऐसे दल लोकतंत्र का रोना रोते हैं।
भारत में क्षेत्रीय विविधता है। समाज में सैकड़ों जातियां, उप जातियां हैं। समाज जातियों, उप जातियों में विभाजित है। विचारहीन दल उपजातियों जातियों के आधार पर दल बनाते हैं। जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। कायदे से सभी दलों को अपनी विचारधारा के अनुसार लोकमत बनाना चाहिए। विचार आधारित राजनैतिक शिक्षण से ही लोकतंत्र की मजबूती है। दरअसल भारत का आमजन राजनैतिक नहीं है। चुनाव के अलावा शेष समय जनता राजनैतिक व्यवहार से मुक्त रहती है। गांधी जी ने 1895 में लिखा था, ‘भारतीय साधारणतया राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करते’। आमजन अपने स्वभाव से ही राजनीति के प्रति उदासीन हैं। भारतवासी केवल चुनाव के दिनों में ही राजनैतिक दलों द्वारा राजनैतिक रूप में सक्रिय होते हैं।
विचार से दल बनते हैं। दल विचार को आमजनों तक ले जाते हैं। चुनाव में नीति कार्यक्रम व राष्ट्र संवर्द्धन की चर्चा जरूरी है। लेकिन यहां शत्रु राष्ट्र को भी लाभ पहुंचाने वाली बयानबाजी के दुस्साहस दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनतंत्र बेशक परिपक्कव हो रहा है। लेकिन चुनाव अभियानों में शब्द मर्यादा का संयम नहीं है। लोकतंत्र शब्द सौंदर्य से ही मजबूत होता है।