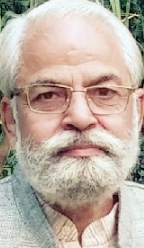
जाने-माने पर्यावरणविद, कालजयी पुस्तक ‘आज भी खरे हैं तालाब’ के रचियेता, समाजवादी युवजन सभा,जेपी आंदोलन, चिपको आंदोलन और चंबल के दस्युओं के आत्म समर्पण में अहम भूमिका निबाहने वाले भाई अनुपम मिश्र जी को इस नश्वर संसार को छोड़े चार वर्ष बीत चुके हैं। पर्यावरण जगत से जुड़े सभी साथी उनको अपनी भावभीनी श्रृद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें सच्ची श्रृद्धांजलि यह होगी कि उनकी कालजयी पुस्तक पर चिंतन-मनन किया जाए जो तालाबों के इतिहास, महत्ता और उपयोगिता के संदर्भ में मील का पत्थर है। अपनी इस पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब में आज से सत्ताइस बरस पहले उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे यहां तालाबों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण यह था कि पुराने तालाब साफ नहीं कराए गए और नए कभी बने ही नहीं।
दरअसल साद तालाबों में नहीं, नए समाज के माथे में भर गई है। उनके कहने का मतलब साफ था कि तब समाज का माथा साफ था, उसने साद को समस्या की तरह नहीं, बल्कि साद को तालाब के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया था। उनके अनुसार सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई, दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले दो सौ बरसों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ा़ई पढ़ गए समाज ने इस इकाई, दहाई, सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। नतीजा सबके सामने है कि जिस देश में तकरीब बीसियों लाख तालाब थे, वहां तालाब आज इतिहास की वस्तु बनकर रह गए हैं।
पानी के मामले में हमारे समाज के जुड़ाव का इसी से पता चलता है कि वह हर परिस्थिति में भी अपने जीवन की रीत खोजने में लगा रहता था। यही नहीं मृगतृष्णा को झुठलाते हुए भी जगह-जगह पानी के तरह तरह के प्रबंध करता रहता था। राजस्थान इसका प्रमाण है। वहां जहां तालाब नहीं, पानी नहीं, वहां गांव नहीं। मतलब साफ है कि तालाब का काम पहले होगा तब उसको आधार बनाकर गांव बसेगा। तात्पर्य यह कि मरुभूमि में सैकड़ों गांवों का नामकरण वहां बने तालाबों के नाम से जड़ा है। जैसलमेर जहां एक भी बारामासी नदी नहीं है, जहां 70 सालों का अध्ययन बताता है कि साल के 365 दिनों में से 355 दिन सूखे गिए गए। मरुभूमि के लोगों ने दस दिन की वर्षा में करोड़ों बूंदों को देखा और उनको घर-घर, गांव-गांव, शहर-शहर एकत्र करने का काम किया। परिणामत: जैसलमेर जिले में 99.78 फीसदी गांवों में तालाब, कुएं आदि अन्य स्रोत हैं। अंग्रेजों के दौर में भी देश में तालाबों पर चल रहे कामों, उनके निर्माण का उल्लेख मिलता है। 1907 तक यह काम चलता रहा। मध्य प्रदेश के दुर्ग और राजनांदगांव इसके उदाहरण हैं। लेकिन यह स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं थी।
पानी पर राज और गुणी समाज के संबंध और प्रबंध को मैसूर राज में सबसे पहले छीनने का प्रमाण मिलता है। गौरतलब है कि 1800 तक मैसूर में पानी और तालाबों की देखरेख राज्य के दीवान पूर्णय्या देखते थे। उस समय अकेले मैसूर राज्य में 39000 तालाब थे, जिनकी देखरेख पर राज के अलावा समाज भी कुछ लाख रुपये हर साल खर्च करता था। अंग्रेजों ने आने के बाद 1831 में राज की ओर से तालाबों की देखभाल के लिए दी जाने वाली राशि आधी कर दी। इसके बाद भी समाज ने 32 सालों तक तालाबों की बखूबी देखभाल की। इसके बाद 1863 में पीडब्ल्यूडी विभाग बनते ही तालाबों की देखभाल का जिम्मा समाज से ले लिया गया। ऐसी स्थिति में धन, साधन और स्वामित्व के बिना समाज लाचार हो गया और तालाबों का प्रबंधन कभी पीडब्ल्यूडी तो कभी सिंचाई विभाग के बीच झूलता रहा लेकिन राजस्व बढ़ता रहा और तालाबों के रखरखाव का मामला कभी चंदा तो कभी जबरन बसूली के बीच उलझा रहा। हालत यह हो गयी कि तालाब लाभ-हानि के पचडे़ में फंसकर राज के पलड़े से बाहर कर दिए गए।
उसके बाद देश में राजधानी दिल्ली ही नहीं महानगरों में वाटर वर्क्स के जरिये नलों से लोगों को पानी की आपूर्ति की जाने लगी। नतीजतन जगह-जगह नलों का जाल बिछता चला गया और पानी आपूर्ति के मुख्य स्रोत तालाब-कुएं-बावड़ी उपेक्षित होते चले गए। आजादी बाद तो इन जल स्रोतों पर अवैध कब्जों का सिलसिला शुरू हुआ और इनपर मकान, आवासीय कालोनियों का जाल बिछता चला गया। दुखदायी बात यह कि जल की निकासी की व्यवस्था की ओर नगर नियोजकों का ध्यान ही नहीं गया जिसका परिणाम बारिश के दौरान शहरों के डूबने के रूप में सामने आया। सत्तर के दशक के बाद तो अधिकांश तालाबों का देश में नामोनिशान तक नहीं रहा और उनपर कहीं स्टेडियम, कहीं बाजार और मोहल्ले दिखाई देने लगे। नगर पालिकाएं, नगर निगम शहरवासियों को वाटर वर्क्स के जरिये पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ दिखाई देने लगे। जल संकट गहराने लगा। नतीजतन लोग बोरिंग कर मोटर पम्पों, ट्यूबवैल के जरिये पानी की जरूरत पूरी करने लगे। जिसका दुष्परिणाम भूजल के भीषण संकट के रूप में हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है।
दरअसल, पानी के मामले में निपट बेवकूफी के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर का उदाहरण हमारे सामने है। कोई छह सौ बरस पहले लाखा बंजारे द्वारा बनाए गए सागर नामक विशाल तालाब के किनारे बसे शहर का नाम सागर ही हो गया था। आज यहां नए समाज की पांच बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। जिले और संभाग के मुख्यालय हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। सेना का महार रैजिमेंटल सेंटर है। सेना के कई डिवीजन के मुख्यालय हैं। नगर पालिका है। डा.सर हरीसिंह गौर के नामपर बना विश्व विद्यालय है। एक बंजारा यहां आया और विशाल सागर बनवाकर चला गया। लेकिन नए समाज की ये साधन संपन्न संस्थाएं इस सागर की देखभाल तक नहीं कर पार्इं। एक अनपढ़ माने गए बंजारे के हाथों बने सागर को पढ़ा-लिखा माना गया समाज बचा तक नहीं पा रहा है। असलियत में पानी,पर्यावरण व समकालीन सामाजिक सरोकारों में गांधीवादी समझ व मूल्यों को अपने जीवन में उतारने वाले चिंतक, लेखक, अहिंसक योद्धा और मौजूदा पीढ़ी के महान गांधीवादी भाई अनुपम जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं)
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1



