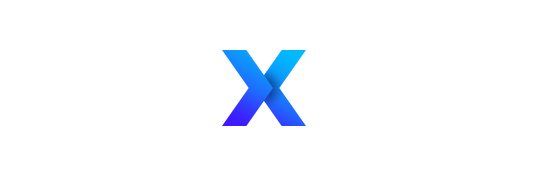घर में आटा चुक गया था। दफ़्तर से लौटने पर मनोहर को पहला हुक्म गेहूं पिसा लाने का मिला। दस सेर गेहूं साफ करके एक गंदी-सी टोकरी में रख दिए गए थे। यह काम करना ही पड़ेगा-सोच मनोहर ने एक गहरी सांस खींची।
घर में आटा चुक गया था। दफ़्तर से लौटने पर मनोहर को पहला हुक्म गेहूं पिसा लाने का मिला। दस सेर गेहूं साफ करके एक गंदी-सी टोकरी में रख दिए गए थे। यह काम करना ही पड़ेगा-सोच मनोहर ने एक गहरी सांस खींची।
नया-नया बीए किया था, यद्यपि शादी पहले हो चुकी थी। नई-नई नौकरी आरंभ की थी और गृहस्थी का हिसाब भी नया ही था। थोड़ी तनख़्वाह में किसी प्रकार मनोहर अपनी बीवी और दुधमुंहे बच्चे के साथ-साथ अपनी बाबूगिरी को भी पाल रहा था। गंदे कपड़े पहनने वाले, बंद गले के कोट और गोल टोपी में आने वाले पुरनिया बाबुओं को वह शासन के सर्वथा अयोग्य समझता था।
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दस सेर गेहुओं को देखकर उसे लगा मानो दसों दिशाएं उसके ऊपर चारों ओर से चिंता की धारा बरसा रही हैं।
गेहूं लेकर रास्ते से निकलना है। अगर रास्ते में मि. भारद्वाज मिल गए तो? कल इतवार है, सवेरे उन्होंने चाय पर बुलाया है। विश्वविद्यालय के पुराने साथी हैं। असिस्टेंट राशनिंग अफसर हो गए हैं, फिर भी मित्रता मानते हैं। ये गेहूं किसी मजदूर को भेजकर पिसा लिए जाएं।
पर विश्वास योग्य मजदूर मिले कहां? और आटा चक्की भी कोसों दूर है। कोई मिला भी तो आठ-दस आने से कम क्या लेगा? जितने की भगति नहीं उतने की खंजड़ी फूट जाएगी। फिर दस सेर गेहूं के लिए मजदूर-यह जानते ही अन्नपूर्णा का मितव्ययता पर भाषण कौन सुनेगा? एक तरकीब सूझी। गेहूं का वजन इतना कर लिया जाए कि मजदूर अनिवार्य हो जाए। बोला, ‘यह रोज-रोज का झंझट मुझे ठीक नहीं लगता। सब गेहूं निकाल लो, अभी पिसवा मंगाऊंगा।’
अन्नपूर्णा ने सीधी निगाहों से देखकर कहा, ‘जाकर पिसा लाओ। आधे घंटे का काम है। और गेहूं नहीं है।’
अन्नपूर्णा ने एक मैले झोले में, जिसे पुरानी साड़ियों के किनारों को जोड़-जोड़कर बनाया गया था, गेहूं भर दिए; कहा, ‘ले जाओ।’
मनोहर ने झल्लाकर कहा, ‘ए, वह झोला मैं छुऊंगा भी नहीं। ओह! कितना गंदा है।’
अपेक्षाकृत एक साफ धोती थी। उसे दोहरा कर उसमें गेहूं बांधे गए। एक छोटी-सी पोटली बन गई। अब उसे बगल में दबाने पर जान पड़ा कि वह कमीज के सामने काफी मैली पड़ती है। मनोहर ने घर पर पहनने वाली यानी मैली कमीज और उतनी ही मैली धोती पहन ली। चलते-चलते कहा, ‘मेरी सिल्क वाली कमीज के बटन टूट गए हैं, लगा देना। कल उसे ही पहनकर एआरओ साहब के यहां चाय पर जाना है।’
इतना कहकर बाहर आया। झुका-झुका सड़क पर चलने लगा। दस सेर गेहूं क्या लिए जा रहा था, मानो इतने ही गेहूं कहीं से चुराकर, लोगों की निगाह बचाकर, भागा जा रहा था।
जो डर था वही सामने आया। बाबू श्यामनाथ, भारद्वाज के भाई, सामने से टहलते हुए आ रहे थे। मनोहर की बार-बार इच्छा हुई कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। शंका यह है कि यह इच्छा एक बार भी क्यों न हुई कि जमीन फटे और स्वयं बाबू श्यामनाथ उसमें समा जाएं। समाधान यह है कि यदि ऐसा हो भी जाता तब भी मनोहर अपनी पोटली के साथ पृथ्वी की लज्जा का भार सहन करने के लिए रह ही जाता।
पर जमीन इतनी सस्ती नहीं है कि इच्छा करते ही टके की पतंग की तरह फट जाए। बाबू श्यामनाथ सामने आ गए।
वे शायद मनोहर को देखते भी नहीं, पर उसने सोचा कि यदि उन्होंने देख लिया तो समझेंगे कि वह इस हालत में मारे झेंप के चुपचाप निकला जा रहा है। इस कारण, यह सिद्ध करने के लिए कि अपना काम करने में वह जहाज पर कोयला झोंकने वाले प्रिंस आॅफ वेल्स ही-सा महान और निर्लज्य है, उसने पहले ही कहा, ‘ओ हो, श्यामनाथ जी हैं? कहां?’
उनकी स्वाभाविक मुस्कान भी उसे व्यंग्यभरी जान पड़ी। उन्होंने पूछा, ‘आप कहां?’
‘अरे साहब, ये गेहूं गले पड़ गए। अभी पिछले इतवार को वह लौंडा पच्चीस सेर के करीब पिसा ले गया था। सब न जाने कहां चला गया! सोचा, फिलहाल के लिए इतना पिसा लाऊं।’
‘भेज देना था किसी को। चलिए, ‘रतन’ देख आएं। ऐसी पिक्चर आज तक नहीं बनी।’
‘अरे जनाब, रतन देखने की फुरसत कहां है!’ कहते ही उसे लगा कि उसने पुराने बाबुओं वाली कोई बात कह दी है। चलते-चलते श्यामनाथ जी कह गए, ‘कल आइएगा अवश्य। मिस आहूजा भी शायद आवें।’
श्यामनाथ की आवाज! उसे लगा कि उसमें कुछ रुखाई-सी है।
और, मिस आहूजा?
कहां दस सेर गेहूं और कहां वे! केवल रंग की समता है।
बैसाख के सूरज की ढली रोशनी में चक्की के सामने रूखा दृश्य, आटे के कणों से भरी हुई हवा का स्पर्श, घर्र-घर्र का घोर शब्द, मुंह खोलते ही खांसी लाने वाला रस, लोगों के पसीने की गंध। समस्त ज्ञानेंद्रियों को सुन्न करने वाला यह वातावरण उसे मिस आहूजा के बारे में रोमांटिक नहीं बना पाया। एक विचार मन में घुस गया था, वह कल सिल्क वाली कमीज पहनकर जाएगा जरूर, पर क्या श्यामनाथजी उसका आज का रूप भूल सकेंगे?
जब उसने बार-बार चक्कीवाले से आटा पीसने में जल्दी करने को कहा तो उसने अपने क्षेत्र में सुमान्य, युद्धोत्तर सभ्यता के नियम का पालन करते हुए कहा, ‘जल्दी हो तो कहीं और जाओ। वे रहे तुम्हारे गेहूं।’
झेंपकर मनोहर एक कोने में खड़ा हो गया। वहीं प्राय: पैंतालीस साल का एक मैला-सा आदमी खड़ा था। वह पांवों तक कसा हुआ पाजामा पहने था। बदन पर कुर्ता था जो जरूरत से ज्यादा लंबा और कंधों पर फटा हुआ था। कुछ दाढ़ी बढ़ गई थी। गाल के गढ्डों और कनपटियों के ऊपर बालों में सफेदी आ गई थी। आंखें डरावनी और फूली हुई लग रही थीं। वह बीड़ी पी रहा था। उसने एक फूंक मनोहर की ओर फेंककर पूछा, ‘कहां काम करते हो?’
मनोहर को उससे बात करने में अपमान-सा जान पड़ा। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब वह आगे बढ़ आया और मनोहर के मुंह में झांककर अपना सवाल दोहराते हुए बोला, ‘कहाँ काम करते हो?’
अनिच्छा के साथ मनोहर ने बताया, ‘सीओडी में।’
‘ठीक। मैं पहले ही जान गया था।’
‘कैसे?’ मनोहर ने घूरते हुए पूछा।
उसने अपना सर जोकरों की भांति हिलाकर पास खड़े हुए अपने दो-तीन साथियों से कहा, ‘जो बहुत जल्दी मचाए तो जान लो कि वह दस घंटा सीओडी में मजदूरी करके आया है।’ पता नहीं इसमें क्या बात थी कि वे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मनोहर कुपित नेत्रों से उसे देखता रहा।
उसने पूछा, ‘क्या पाते हो?’
मनोहर ने लापरवाही से कहा, ‘मिल जाता है खाने-भर को।’
उसने फिर अपना भयंकर सिर जोकरों जैसा हिलाया और अपने साथियों से बोला, ‘अरे जान लो भाई लोगो, सीओडी में भी एक आदमी खाने-भर को पा जाता है।’ फिर उसने मनोहर से पूछा, ‘क्यों जी, खाने-भर को तो मिल जाता है, पहनने-भर को भी मिलता है कि नहीं?’
मनोहर ने कुछ कहना चाहा, मुंह खोला। फिर चुप हो गया।
उसने फिर पूछा, ‘डेढ़ रुपया रोज मिलता है?’
मनोहर ने कहा, ‘मैं तीन रुपया रोज पाता हूं। पर तुमसे मतलब?’
इस पर वह आदमी फिर अपने साथियों के साथ हंस पड़ा। मनोहर के मन में आया कि वह उनकी खोपड़ी तोड़ दे, पर परिस्थिति समझकर चुपचाप खड़ा रहा।
हंसी रुकने पर उस आदमी ने कहा, ‘मतलब तो मुझको कुछ नहीं है। तुम तो बाबू हो बाबू। तुम्हें तीन रुपया रोज मिलता है। मुझको तुमसे क्या मतलब?’
अब मनोहर ने जरा कड़ाई से कहा, ‘देखो जी, मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं।’
वह अपने साथियों से बोला, ‘इन्हें भला क्यों पसंद आएगा हमारा मजाक। ये ठहरे बाबू, तीन रुपिया रोज वाले। हम लोग ठहरे लट्ठ गंवार! मजदूर! हमारा मजाक इन्हें क्यों अच्छा लगेगा?’
अपने एक साथी से उसने पूछा, ‘क्यों रे, तेरा लड़का भी तो इंट्रेस में पढ़ता है?’
साथी ने कहा, ‘जानते तो हो।’
यह आदमी कहने लगा, ‘देख बे, उस छोकरे को इंट्रेंस न पास करा। नहीं तो वह भी बाबू बनकर अपने लोगों से अलग हो जाएगा। तनख़्वाह मिलेगी साले को सत्तर रुपल्ली, पर समझेगा कि वह तुझसे हजार गुना ऊंचा है। वह तेरी नकल न करेगा। वह नकल करेगा अफसरों की, सेठ-साहूकारों की। इसी बाबू की तरह बात करने पर नाक-भौं चढ़ाएगा। वह भी भूल जाएगा कि उसकी जड़ कहां है।’
वे सब हंसते रहे।
मनोहर ने पढ़े-लिखे आदमी की तरह समझ लिया कि संधि करने में ही कल्याण है। बोला, ‘क्या बात है जी? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम यह सब कहने लग गए?’
मनोहर की आवाज ही संधिपत्र था। उस पर उस आदमी ने भी हस्ताक्षर करने चाहे। वह नर्मी से बोला, ‘बात कुछ नहीं है बाबू, सिर्फ़ समझ का फेर है। तभी मेरे पहले सवाल करने पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। तभी जेब खाली होने पर भी रेल में ऊंचे दर्जे का सफर करते हो ताकि कहीं हमारे जिस्म की हवा, हमारी तंबाकू की गंध तुम्हें छू न जाए। तभी तुम उन जगहों में पहुंचने की कोशिश करते हो जहां तुम्हारा कोई नहीं है।’
इस बार लोग हंसे नहीं। चक्की की घर्राहट के बीच ड्राइवर की अशिष्ट आवाज सुन पड़ी, ‘लो जी, गेहूं पिस गए, निकालो ढाई आने।’
पैसे देकर, हाथ में आटा लटकाकर, वह बाहर आया। उस आदमी ने इस बार मनोहर की ओर नहीं देखा। वह बीड़ी सुलगाने में व्यस्त था। मनोहर को संदेह हुआ कि वह कुछ पढ़ा-लिखा आदमी है, जानने योग्य है। पर हिचक के मारे वह चुपचाप चला आया।
घर आकर, आटा एक किनारे रख, नहाने चल दिया। अन्नपूर्णा ने रोककर सिल्क की कमीज उसके हाथों में रख दी और पूछा, ‘कुछ और ठीक करना है?’
एक पल वह अन्नपूर्णा के पीले और मुरझाए चेहरे की ओर देखता रहा। उसके बाद धुएं से धूमिल आंगन पर उसने निगाह डाली। नीचे अंधेरा था, पर दुमंजिÞले के ऊपर मुंडेरों पर, जहां अधिक किराया देने वालों ही की पहुंच थी, सूरज पूरी तरह अभी डूबा न था। उसकी लाल रोशनी अब भी छतों पर फैल रही थी।
उसने फिर अन्नपूर्णा के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा कि वह चेहरा उसने बहुत दिन बाद देखा है। फीकी मुस्कान के साथ उसने एक उंगली अन्नपूर्णा की ठुड्डी पर आवेग के साथ फेरी और कहा, ‘और कुछ नहीं ठीक करना।’
फिर तौलिया और साबुन जमीन पर रखकर, कपड़ों का पुराना संदूक खोल उस कमीज को उसमें सबसे नीचे रख दिया। उसके बाद नहाने गया।
श्रीलाल शुक्ल