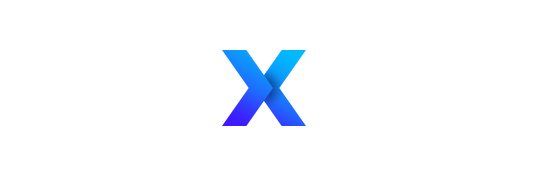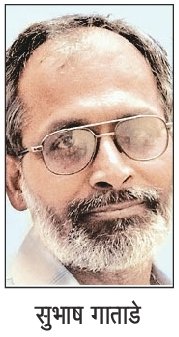 ‘पुस्तकालय का अर्थ शीतगृह में रखा गया कोई विचार’, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हर्बर्ट सैम्युअल का यह विचार काफी दूरदर्शी लगता है, लेकिन फिलवक्त उसका कोई असर राष्ट्रीय राजधानी की 161 साल पुराने पुस्तकालय की नियति पर पड़ता नहीं दिखता, जिसे अचानक दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, बिजली का बिल जमा न हो पाने के चलते जिसकी बिजली काट दी गई है और कर्मचारी बिना तनखाह के काम कर रहे हैं। वैसे लाला हरदयाल नाम के महान स्वतंत्राता सेनानी और विद्धान के नाम से बने इस पुस्तकालय के समस्याओं की जड़ फिलवक्त उसका प्रबंधन करनेवाले लोगों के आपसी विवादों में देखी जा रही है। मालूम हो कि इस ऐतिहासिक पुस्तकालय में 1,70,000 से अधिक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन और संस्क्रत ग्रंथ हैं… दुनिया के उन गिने चुने पुस्तकालयों में यह शुमार है जहां बहुत दुर्लभ श्रेणी में गिनी जाने वाली 8000 दुर्लभ किताबें भी हैं। बताया जाता है कि एक शख्स जो कभी ग्रंथालय के संचालन के लिए बनी कमेटी के प्रमुख सदस्य रहे हैं तथा हिंदुत्व वर्चस्ववादी नजरिये के प्रति उनकी सहानुति जगजाहिर है-उनके अडियलपन के चलते यह अभूतपर्व स्थिति बनी है। मुमकिन है कि आप जब इन पंक्तियों को पढ़ रहे हों, तब तक स्थिति बदल गई होगी और वह ऐतिहासिक पुस्तकालय धीरे-धीरे अपने सामान्य रास्ते पर चल रहा हो।
‘पुस्तकालय का अर्थ शीतगृह में रखा गया कोई विचार’, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हर्बर्ट सैम्युअल का यह विचार काफी दूरदर्शी लगता है, लेकिन फिलवक्त उसका कोई असर राष्ट्रीय राजधानी की 161 साल पुराने पुस्तकालय की नियति पर पड़ता नहीं दिखता, जिसे अचानक दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, बिजली का बिल जमा न हो पाने के चलते जिसकी बिजली काट दी गई है और कर्मचारी बिना तनखाह के काम कर रहे हैं। वैसे लाला हरदयाल नाम के महान स्वतंत्राता सेनानी और विद्धान के नाम से बने इस पुस्तकालय के समस्याओं की जड़ फिलवक्त उसका प्रबंधन करनेवाले लोगों के आपसी विवादों में देखी जा रही है। मालूम हो कि इस ऐतिहासिक पुस्तकालय में 1,70,000 से अधिक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन और संस्क्रत ग्रंथ हैं… दुनिया के उन गिने चुने पुस्तकालयों में यह शुमार है जहां बहुत दुर्लभ श्रेणी में गिनी जाने वाली 8000 दुर्लभ किताबें भी हैं। बताया जाता है कि एक शख्स जो कभी ग्रंथालय के संचालन के लिए बनी कमेटी के प्रमुख सदस्य रहे हैं तथा हिंदुत्व वर्चस्ववादी नजरिये के प्रति उनकी सहानुति जगजाहिर है-उनके अडियलपन के चलते यह अभूतपर्व स्थिति बनी है। मुमकिन है कि आप जब इन पंक्तियों को पढ़ रहे हों, तब तक स्थिति बदल गई होगी और वह ऐतिहासिक पुस्तकालय धीरे-धीरे अपने सामान्य रास्ते पर चल रहा हो।
गौरतलब है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की बढ़ती उपेक्षा की यही एकमात्र मिसाल नहीं है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देखें तो वहां पर भी हाल के महिनों में ऐसी ही मिसाल सामने आई थी, जब वहां के बहुचर्चित सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज (इतिहास अध्ययन विभाग) के पुस्तकालय पर संकट के बादल मंडराते दिखे थे। अचानक यह खबर मिली थी कि इतिहास अध्ययन पर केंद्रित इस ग्रंथालय को-जिसकी खासियत यह रही है कि यहां के किताबों के संग्रह और विभिन्न मोनोग्राफ काफी उच्च स्तरीय समझे जाते हैं, (जिसमें प्रख्यात विद्वान डीडी कोसाम्बी जैसे कई के किताबों का पूरा संग्रह उसे अनुदान में मिला है) इतना ही नहीं यहां के किताबों से लाभान्वित होकर प्रगतिशील इतिहासकारों की पीढ़ियां तैयार हुई हैं, उसे वहां से शिफ्ट किया जाएगा और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था।
ग्रंथालय को जिस एक्जिम लाइब्रेरी में शिफ्ट किया जाना था, वहां पर पहले से ही जगह का संकट था, जो खुद छोटी जगह थी। जानकारों को यह पता करने में अधिक वक्त नहीं लगा कि ऐसे छोटे स्थान पर अगर लाइब्रेरी को शिफ्ट किया गया तो कई सारी पुरानी किताबें, मोनोग्राफ बरबाद हो जाएंगे और इतना ही नहीं, इतिहास के अध्येताओं के लिए भी इस लाइब्रेरी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर साहित्य बंधा रह जाएगा। विश्वविद्यालय के छात्रों-अध्यापक ही नहीं देश-दुनिया के अन्य विद्वानों द्वारा जब इस शिफ्टिंग पर सवाल उठाया गया तब फिलवक्त उसे रोक दिया गया है। यह मालूम नहीं कि नोटिफिकेशन वापस लिया गया या नहीं? मुमकिन है अगर विरोध की आवाजें मद्धिम हों या ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की आबादी कम हो, प्रशासन अपने इस फरमान पर अमली जामा पहना दे।
चाहे सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज का स्थापित पुस्तकालय हो या ऐतिहासिक लाला हरदयाल लाईब्रेरी हो, हम यही देखते हैं कि विगत लगभग एक दशक से दक्षिण एशिया के इस हिस्से में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें बदलते सियासी वातावरण में-जब सत्ताधारियों के सरोकार अलग किस्म के हैं – अलग किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब एक प्रस्तावित विधेयक के चलते उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इस विधेयक के तहत सार्वजनिक पुस्तकालयों को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल करने की योजना है। मालूम हो कि समवर्ती सूची में वह मसले शुमार होते हैं, जिसमें केंद्रऔर राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी मानी जाती है।
इस सम्बन्ध में अधिक चिंतनीय मसला यह भी है कि केंद्र में सत्तासीन हुकूमत इस प्रस्ताव को गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाती दिखी है ताकि इस मामले में अधिक शोरगुल न हो, राज्य सरकारों की तरफ से इस बिल के औचित्य को लेकर नई बहस न खड़ी हो और फिर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन में केंद्रीय हुकूमत की दखलदाजी के लिए भी रास्ता खुल जाए।
एक, अहम बात यह लगती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उससे सम्बद्ध संगठन जैसे भाजपा हो या अन्य आनुषंगिक संगठन हों, उनका अपना चिंतन सार्वजनिक पुस्तकालय के विचार के बिल्कुल खिलाफ पड़ता है। जिस किस्म के असमावेशी विचार को, नजरिये को वह बढ़ावा देते हैं वह सार्वजनिक पुस्तकालय के विचार का विरोध है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि हर दक्षिणपंथी विचारधारा या जमातें ऐसे पाठयक्रमों से या किताबों से इतना डरते क्यों हैं, जो व्यापक जनसमुदाय में खोज करने, सवाल पूछने की प्रवृत्ति को तेज करे। भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों को रफता रफता केंद्र सरकार के अधीन लाने की यह कोशिश दो अनुभवों की याद दिलाती है।
दरअसल इतिहास इस बात की ताईद करता है कि हिटलर के युग में नात्सी हुकूमत ने इसी किस्म की कोशिश की थी। इस प्रयोग पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें एक किताब अधिक चर्चित हुई है जिसका लेखन मागार्रेट स्टीग किताब का शीर्षक है ‘पब्लिक लाइब्रेरीज इन जर्मनी’ जो इस प्रोजेक्ट की अहम विशेषताओं को रेखांकित करती है।
लेखिका के मुताबिक नात्सी परियोजना का ‘केंद्रीय हिस्सा था सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से सूचनाओं को ज्ञान के प्रसार का’ एक तरह से कहें तो ‘नात्सी सार्वजनिक ग्रंथालय एक तरह से राजनीतिक सार्वजनिक पुस्तकालय’ को परिभाषित करता था। मालूम हो अपनी विचारधारा को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए नात्सी हुकूमत ने सार्वजनिक पुस्तकालयो के ताने बाने का विस्तार भी किया। भारत की ओर लौटें तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के नए रूपरंग में ढालने की हिंदुत्व विचारों के वाहकों की बेचैनी या बदहवासी समझी जा सकती है।
एक तरफ यह एक ऐसा समय है, जब खुद प्रधानमंत्री 2014 में सत्तारोहण के बाद से ही ‘भारत की हजार साला गुलामी’ की बात करते दिखते हैं, जो संघ-भाजपा के दृष्टिकोण का विस्तार है, अलबत्ता 1947 के बाद आजादी के इतिहास पर इतना जो कुछ लिखा गया है, उससे यह समझदारी बिल्कुल विपरीत है। हकीकत यही है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की गुलामी का दौर लगभग डेढ़ सौ साल रहा है। विगत कुछ सालों से यह सचेतन कोशिश चल रही है कि एक ऐसे आख्यान को वैधता प्रदान की जाए, जो हिंदुत्व के विश्व नजरिये के अनुकूल हो। शायद इस पृष्ठभूमि में संघ भाजपा के लिए यही रास्ता मुफीद लग रहा है कि कि वह सार्वजनिक पुस्तकालयों पर अपना कब्जा कायम करे और अपनी इस एकांगी समझदारी को अधिक विस्तार दे, उसके पक्ष में जनमत तैयार करे।