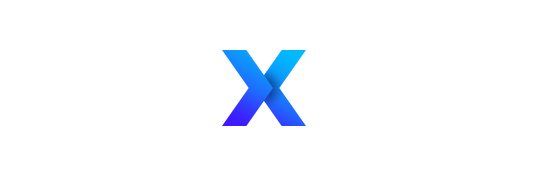- Advertisement -
 स्वाधीनता के पूर्व हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए आत्याचार, शोषण का शिकार हुए, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी हम अपने ही चुने हुए सरकार के भ्रष्टाचार के शिकार हैं। स्वतंत्रता के पूर्व लोगों के मन में यही आस थी कि अंग्रेजों को भगाकर हम अपनी सरकार बनाएंगे, जिसमें जिस सरकार में हमारे अपने भाई और हम राज करेंगे, जिसमें हर प्रकार कि स्वतंत्रता सभी को प्राप्त होगी, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। हमारी अपनी सामूहिक शक्ति शासन को चलाएंगी स्वतंत्र भारत का निर्माण होगा, किंतु आज आजादी के इतने वर्षों बाद हम सब देख रहे हैं कि यह लोकतंत्र किस हद तक जनता का बना रह सका है।
स्वाधीनता के पूर्व हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए आत्याचार, शोषण का शिकार हुए, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी हम अपने ही चुने हुए सरकार के भ्रष्टाचार के शिकार हैं। स्वतंत्रता के पूर्व लोगों के मन में यही आस थी कि अंग्रेजों को भगाकर हम अपनी सरकार बनाएंगे, जिसमें जिस सरकार में हमारे अपने भाई और हम राज करेंगे, जिसमें हर प्रकार कि स्वतंत्रता सभी को प्राप्त होगी, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। हमारी अपनी सामूहिक शक्ति शासन को चलाएंगी स्वतंत्र भारत का निर्माण होगा, किंतु आज आजादी के इतने वर्षों बाद हम सब देख रहे हैं कि यह लोकतंत्र किस हद तक जनता का बना रह सका है।
लोकतंत्र को बनाने और उसे बनाए रखने में साहित्यकार की विशिष्ट भूमिका होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के साहित्य की भूमिका निर्विवाद है। हर देश का साहित्य वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पक्षों से प्रभावित होता है। और इसकी तस्वीर वहां के साहित्य में परिलक्षित होती है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक तंत्र और स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र में बहुत बदलाव आ चुका है। चूंकि स्वतंत्रता के पश्चात साहित्यकारों की भूमिका उत्तरोत्तर और अधिक महत्वपूर्ण हुई है। सामाजिक एवं राजनीतिक भटकावों और भारतीय जनता के सपनों में बाधक बने तत्वों को साहित्य का विषय बनाकर साहित्यकारों ने इस पर अपनी भरपूर लेखनी चलाई है।
‘साहित्यकारों का लोकतंत्र समता, स्वाधीनता और बंधुत्व पर आधारित होता हैं एक ऐसे संवेदनशील लोकतंत्र की स्थापना साहित्यकारों का उद्देश्य रहा है, जो शोषणविहीन हो, जहां जाति, रंग प्रांत एवं धर्म के नाम पर किसी प्रकार के भेदभाव न हों। ऐसे लोकतंत्र में आम-आदमी के सपने फलीभूत होंगे।’
वर्तमान में लोकतंत्र महज शासन की एक प्रणाली (तंत्र) मात्र बनकर रह गया है। इसका स्वाभाविक विकास जीवन-शैली के रूप में आज भी अपेक्षित है। कहा जाता है कि जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका ढांचा विधि-समाज को गढ़ता है, लेकिन जिसकी आत्मा सांस्कृतिक-समाज के गठन की अतृप्त आकांक्षा रखती है।लोकतंत्र को स्थापित करने और उसे बनाए रखने में साहित्यकार की विशिष्ट भूमिका होती है।
लोकतंत्र और साहित्य के संबंधों के विभिन्न स्तर और आयाम का अवधारणात्मक अध्ययन और मानव संबंध के विभिन्न संदर्भ में उनका पूरा विवेचन आज के साहित्य विमर्श की अनिवार्य जरूरतों में से एक महत्वपूर्ण जरूरत है। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त लिखे गए राष्ट्रीय-चेतना से पूर्ण साहित्य की भूमिका निर्विवाद है।
आज के लोकतंत्र और साहित्य पर विचार-विमर्श करना वर्तमान युग में आए परिवर्तन को देखते हुए अनिवार्य हो गया है। जनतंत्र और साहित्यकार ऐसा आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर विचार करना आवश्यक है। किसी विषय का महत्वपूर्ण होना उसकी जीवंतता का निदर्शन करता है। जीवंतता समाज सापेक्ष है, इसलिए समाज के अन्य विषयों के साथ जनतंत्र और साहितयकार पर विचार करना हमारे अपने सामाजिक सरोकारों की गवाही देता है।
इस विषय पर कई प्रकार से विचार हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक जरूरी मैं यह मानती हूं कि जनतंत्र और साहित्यकार के परस्पर संबंधों पर बातचीत की जायें और जनतंत्र में साहित्यकार की भूमिका तय की जाये। वास्तव में ये ऐसे विषय है कि जिन पर लंबे समय से बहस चल रही है, परन्तु कोई निश्चित निष्कर्ष हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं।’
वर्तमान में साहित्यकार पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक एवं जनता की विचारधारा को साहित्यकार ही अपनी लेखनी के माध्यम से विस्तृत और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है और साहित्य के माध्यम से ही जन-जन तक वर्तमान समय में व्याप्त सामाजिक, राजनैतिक विचारधाराएं गंभीरता एवं स्पष्टता के साथ पहुंचती है। जनतंत्र की पहचान जनता के सुख-दुखों से होती है। आज भी भारत में स्वाधीनता की इतनी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग जनतांत्रिक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं।
आज की भारत में गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत गहरी और चौड़ी है। बहुत बड़ी आबादी निरक्षर है और ऐसे हालात में हम निरक्षर जनता से यह कहें कि वे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के निवासी है, और उन्हें अपने जनतांत्रिक अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए, यह सरासर गलत है।
फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने प्रख्यात उपन्यास ‘मैला आंचल’ में कहा था कि ‘गरीबी और जहालत दो ऐसी बीमारी हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।’ ये बीमारियां कितनी दूर तक जा सकती हैं, यह हम सब समझ सकते हैं। निर्धनता, जातिवाद, स्त्री शोषण, सामाजिक वैमनस्य, प्रांतवाद, सांप्रदायिकता, निरक्षरता जैसी अनेक चुनौतियां का सामना आज भारतीय जन-मन को करना पड़ रहा है।
इन समस्याओं के साथ हम किस प्रकार आज के लोकतंत्र में अपने को स्वतंत्र समझे और किस प्रकार इन समस्याओं से मुकाबला करें? ऐसे विषयों पर साहित्यिक रचना करना साहित्यकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।
प्रेमचंद ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘गोदान’ में जिस जिंदगी से परिचय कराया था, वह आज के समय में किस हद तक बदली है, इस बात से हम अनजान नहीं हैं। सरकारों के बड़े-बड़े दावों के बावजूद गरीबी की समस्या हमें लगातार परेशान कर रही है। हम सिर्फ ‘भारत उदय’ और ‘जय हो’ के नारे ही सुनते रह जाते हैं, विभिन्न सरकारें रोजगार गारंटी योजना, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवासीय प्लाट, सस्ते आटा-दाल आदि की आपूर्ति आदि जैसी योजनाओं पर अरबों रुपयों खर्च कर रही है। यह पैसा सरकारी खजाने में करदाता की कमाई के हिस्से के रूप में आया है। यह देखना उचित होगा कि गरीबी दूर करने की सरकारों की कोशिशें वास्तव में कितनी सही और कामयाब रही हैं।
औपनिवेशिक काल में ही भारत में सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। यह एक नकारात्मक, प्रतिक्रियावादी, विस्तृत और बहुमुखी अवधारणा, है, जो विभिन्न अवधारणाओं से मिलकर बनी है। भारतीय परिवेश को इसने नकारात्मक अर्थ में प्रभावित किया। आज भी यह अपने बर्बर रूप में मौजूद है। साहित्य में सांप्रदायिकता का संदर्भ मूलत: संप्रदाय/समुदाय की भावना के तहत प्रकट होता है। रचनाकार अपनी अस्मिता को जाने-अनजाने अपने संप्रदाय/समुदाय से जोड़ लेता है। वहीं से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है।
उसके बाद उस समुदाय के सामुदायिक आधार धर्म, और उस समुदाय की सांस्कृतिक विशेषताओं/पहचानों को स्वर देते हैं। और इसी क्रम में अन्य समुदायों के प्रति उपेक्षा का भाव आ जाता है। यह उपेक्षा भाव धीरे-धीरे ईर्ष्या, वैमनस्य तक पहुंच जाता है। और जब एक समुदाय में अन्य समुदायों के प्रति ईर्ष्या, वैमनस्य आदि भाव उपजते हैं, तब अपनी अस्मिता के जुड़ाव के कारण वह रचनाकार उन भावों का वाहक भी बन जाता है।
भीष्म साहनी के उपन्यास ‘तमस’ में सांप्रदायिक समस्या का सीधा चित्रण है। राही मासूम रजा के ‘आधा गांव’ का गंगोली गांव विभाजन के समय विभाजन की परिस्थितियों से बेखबर रहता है। लेकिन विभाजन का दंश वहां तक पहुंच ही जाता है।
भगवान सिंह का उपन्यास ‘उन्माद’ सांप्रदायिकता और फासीवाद को मनोविकार एवं दमित व्यक्तित्व की विकृत परिणितियों के रूप में प्रस्तुत करता है। गीतांजली श्री का उपन्यास ‘हमारा शहर उस बरस’ में हमारी अकादमी दुनिया की संकटग्रस्तता और अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने वाले यथार्थ की कथा है।
एक साधारण परंपरागत जीवन जीने वाले व्यक्ति की हिंदूवाद की तरफ झुकने की प्रक्रिया को उदय प्रकाश ने अपनी कहानी ‘और अंत में प्रार्थना’ में अभिव्यक्त किया है। इलाहाबाद शहर को आधार बनाकर विभूति नारायण राय ने ‘शहर में कर्फ्यू’ लिखी है जिसमें दिखाया है दंगों के समय किस प्रकार पुलिस अपनी धार्मिक भावना का प्रयोग करती है और उकसाती भी है।
रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ लोकतंत्र के क्षरण की अभिव्यक्ति का दस्तावेज है तो वही ‘हंसो, हंसो, जल्दी हंसो’ उस क्षरण के कारण बढ़ते जा रहे जन-आक्रोश को दबाने के लिए शासक वर्ग द्वारा धीरे-धीरे की जा रही लोकतंत्र की हत्या का दस्तावेज है।
आज के लोकतंत्र में एक प्रभावी लेखक किस प्रकार धीरे-धीरे श्रीहीन हो गया यह देखने को मिल रहा है। साहित्यकार को आज सजग रहकर चुनौतियों से ना घबराते हुए डटकर उसका सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्यकार सदैव विरोध में खड़ा होता है, इसलिए उसकी आवाज ताकतवार होती है। हर युग का साहित्य अपने युग की गवाही देता है, इक्कीसवीं सदी को हमें भी यही गवाही देनी है, इसलिए हमारे उत्तरदायित्व और अधिक व्यापक है-उन्हें पूरा कही हम सच्चे मनुष्य और सच्चे साहित्यकार बने रह सकते हैं- यह बात केवल याद करने की ही नहीं, जीवन में उतारने की है।
What’s your Reaction?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
- Advertisement -